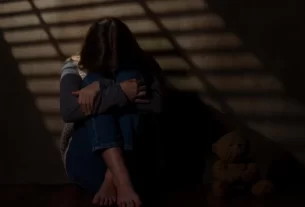हाइलाइट्स
- Fake Social Media ID का इस्तेमाल कर जातियों के बीच नफ़रत फैलाने का आरोप मोहम्मद अहमद पर लगा
- 2020 में गिरफ़्तारी के बाद ज़मानत पर रिहा होकर फिर से सक्रिय हुआ आरोपी
- दर्जनों Fake Social Media ID बनाकर जाट‑गुज्जर, ब्राह्मण‑दलित समुदायों को एक‑दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काया
- हामिरपुर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोबारा जाँच शुरू की; साइबर थाने ने मामला फिर से खोला
- विशेषज्ञों ने चेताया कि Fake Social Media ID ट्रेंड से सामाजिक‑सांस्कृतिक ताने‑बाने पर गहरा ख़तरा मंडरा रहा है
मामले का इतिहास: Fake Social Media ID से शुरू हुई साज़िश
हामिरपुर (उत्तर प्रदेश) पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, जनवरी 2020 में मोहम्मद अहमद को पहली बार तब गिरफ़्तार किया गया था, जब उसने एक Fake Social Media ID बनाकर खुद को जाट बताकर गुज्जर समुदाय के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की थीं। बाद में उसने अलग‑अलग जाति‑धर्म की कम से कम सात Fake Social Media ID तैयार कीं और सुनियोजित ढंग से एक समूह को दूसरे के विरुद्ध उकसाया। पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक, आरोपी ने रामायण और गीता पर भी अश्लील टिप्पणियाँ कीं, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया।
जाँच अधिकारियों ने पुष्टि की कि हर अकाउंट में अलग‑अलग प्रोफ़ाइल फ़ोटो, कवर इमेज और स्थानीय भाषा‑शैली का उपयोग हुआ ताकि असली लग सके। “यह क्लासिक ‘सोशल इंजीनियरिंग’ है—आरोपी ने मनोविज्ञान, भाषा और सांस्कृतिक संकेतों का गहराई से अध्ययन किया,” साइबर सेल के एक अधिकारी ने बताया।
सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की जवाबदेही और Fake Social Media ID
फ़ेसबुक की शुरुआती प्रतिक्रिया
फ़ेसबुक ने शुरुआती शिकायतों पर दो प्रोफ़ाइल तो बंद कर दीं, लेकिन शेष Fake Social Media ID को पहचानने में देर लगाई। कंपनी के प्रवक्ता का कहना था, “हेट‑स्पीच फ़िल्टर और कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स लगातार अपडेट किए जा रहे हैं, पर उपयोगकर्ता रिपोर्टिंग और मानव समीक्षकों का सहयाद महत्वपूर्ण है।”
फ़ैक्ट‑चेक पोर्टल्स की भूमिका
अल्ट न्यूज़ और अन्य फ़ैक्ट‑चेक संगठनों ने अहमद की कई पोस्ट को फ़ेक बताते हुए गहन रिपोर्ट प्रकाशित कीं। इन रिपोर्टों ने आम यूज़र्स को साक्ष्य‑आधारित तरीक़े से समझाया कि Fake Social Media ID किस तरह भाषा और भावनात्मक कंटेंट से विश्वसनीय दिखती है, लेकिन पोस्टिंग पैटर्न और टाइम‑स्टैम्प परखने से भेद खुल सकता है।
कानूनी पहलू: Fake Social Media ID के विरुद्ध कार्रवाई
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153‑A और 295‑A के तहत सांप्रदायिक विद्वेष फैलाना दंडनीय अपराध है। साथ ही, आईटी एक्ट की धारा 66‑F (साइबर आतंकवाद) और 67 (आपत्तिजनक सामग्री) का प्रयोग भी किया जा सकता है। हामिरपुर के पुलिस अधीक्षक का कहना है, “पहली गिरफ़्तारी के समय हमारे पास सीमित डिजिटल फ़ॉरेंसिक क्षमता थी। अब एडवांस्ड डेटा रिट्रीवल टूल्स की मदद से हम हर Fake Social Media ID का आईपी‑लॉग, लोकेशन हॉप और डिवाइस फ़िंगरप्रिंट ट्रैक कर रहे हैं।”
विशेषज्ञ वकीलों का मत है कि अदालत में दोषसिद्धि तभी संभव है जब अभियोजन यह सिद्ध कर सके कि आरोपी की मंशा जानबूझकर नफ़रत फैलाने की थी। “यहाँ डिजिटल फ़ुटप्रिंट, चैट लॉग और मेटा‑डेटा निर्णायक साक्ष्य होंगे,” सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आलोक रंजन बताते हैं। वो मानते हैं कि Fake Social Media ID से निबटने के लिए क़ानूनी ढांचा तो है, पर अमल में लचीलापन और धीमी जांच प्रक्रिया बड़ी बाधाएँ हैं।
समाज पर प्रभाव और Fake Social Media ID का ख़तरा
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जातीय गोलबंदी वाली राजनीति को ऑनलाइन नफ़रत से अप्रत्यक्ष बल मिलता है। “जब कोई Fake Social Media ID दलित बनकर ब्राह्मणों को गाली देती है, तो वास्तविक जीवन में अविश्वास और टकराव बढ़ता है,” लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. सुशील शुक्ला ने कहा।
युवा और डिजिटल नागरिकता
एनसीआरबी डेटा दर्शाता है कि 18‑30 वर्ष के युवा सोशल मीडिया पर सबसे सक्रिय हैं। अधिकांश युवा यह मानते हैं कि ऑनलाइन बयानबाज़ी “वर्चुअल” है, पर जमीनी स्तर पर इसके गंभीर परिणाम दिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विश्लेषक रीमा भटनागर बताती हैं, “परस्पर विरोधी स्क्रीनशॉट शेयर होते‑होते वे चैट ग्रुप्स तक पहुँच जाते हैं, जहाँ आगे की अफ़वाहें फैलती हैं। यहाँ Fake Social Media ID एक ‘स्पार्क’ की तरह काम करती है।”
रोकथाम के उपाय: Fake Social Media ID से निपटने की रणनीतियाँ
- द्विस्तरीय सत्यापन (Two‑Factor Authentication): सोशल नेटवर्क को अनिवार्य बनाना चाहिए कि जाति‑धर्म आधारित पेज़ या समूह बनाने से पहले आधिकारिक आईडी वेरिफ़िकेशन ज़रूरी हो। इससे Fake Social Media ID की संख्या घटेगी।
- एआई‑सहायित मॉडरेशन: भाषा‑विशेष के हेट‑कीवर्ड और “फ़र्श से छत तक” संदर्भित वाक्यांशों की डेटाबेस तैयार कर प्लेटफ़ॉर्म्स को रीयल‑टाइम अलर्ट जारी करना चाहिए।
- डिजिटल साक्षरता अभियान: स्कूल‑कॉलेजों में पाठ्यक्रम के रूप में ‘सोशल मीडिया एथिक्स’ जोड़ना ज़रूरी है ताकि युवा समझ सकें कि Fake Social Media ID कैसे पहचानी जाए।
- क़ानूनी त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र: कम्प्लेंट दर्ज होने के 48 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट द्वारा प्राथमिक आदेश और 72 घंटे में फ़र्स्ट‑इन्फ़र्मेशन रिपोर्ट (FIR) का प्रावधान।
- सिविल सोसाइटी निगरानी: एनजीओ और मीडिया हाउसेज़ द्वारा सामुदायिक ‘हेट‑वॉच’ पोर्टल चलाना, जहाँ संदिग्ध Fake Social Media ID की सूची सार्वजनिक रूप से अपडेट रहें।
मोहम्मद अहमद का मामला महज़ एक व्यक्ति के अपराध से कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है—क्या हम अपने डिजिटल समाज को विश्वासयोग्य बना पाए हैं? Fake Social Media ID किसी भी क्षण हमारी स्क्रीन पर प्रकट होकर हमारे सबसे सूक्ष्म सांस्कृतिक विभाजनों को हथियार बना सकती है। जब तक सोशल मीडिया कंपनियाँ, क़ानून प्रवर्तन एजेंसियाँ और आम उपयोगकर्ता मिलकर जवाबदेही नहीं सुनिश्चित करते, तब तक यह ख़तरा बना रहेगा।
ब्रॉडकास्ट पत्रकार कविता त्रिपाठी के शब्दों में, “अगर 20वीं सदी में पीले पन्नों की अफ़वाहें दंगों का कारण बनती थीं, तो 21वीं सदी का समानान्तर Fake Social Media ID है। फ़र्क़ बस इतना है कि अब यह अफ़वाह एक क्लिक में लाखों लोगों तक पहुँच जाती है।”
इसीलिए आवश्यक है कि हर नागरिक न केवल अपना डिजिटल पदचिह्न संभाले, बल्कि शक होने पर Fake Social Media ID को रिपोर्ट करे, स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखे और तथ्यों की पुष्टि करे। लोकतंत्र में असहमति सहज है, लेकिन असहमति की आड़ में छुपी यह अनदेखी आग हर सामाजिक ताने‑बाने को राख कर सकती है।